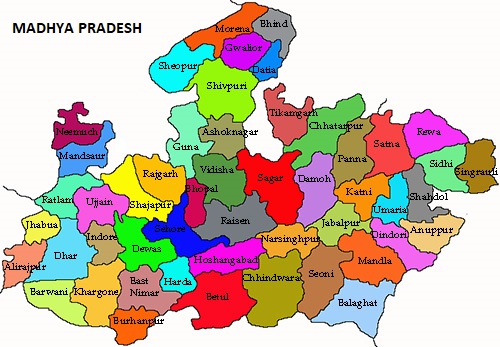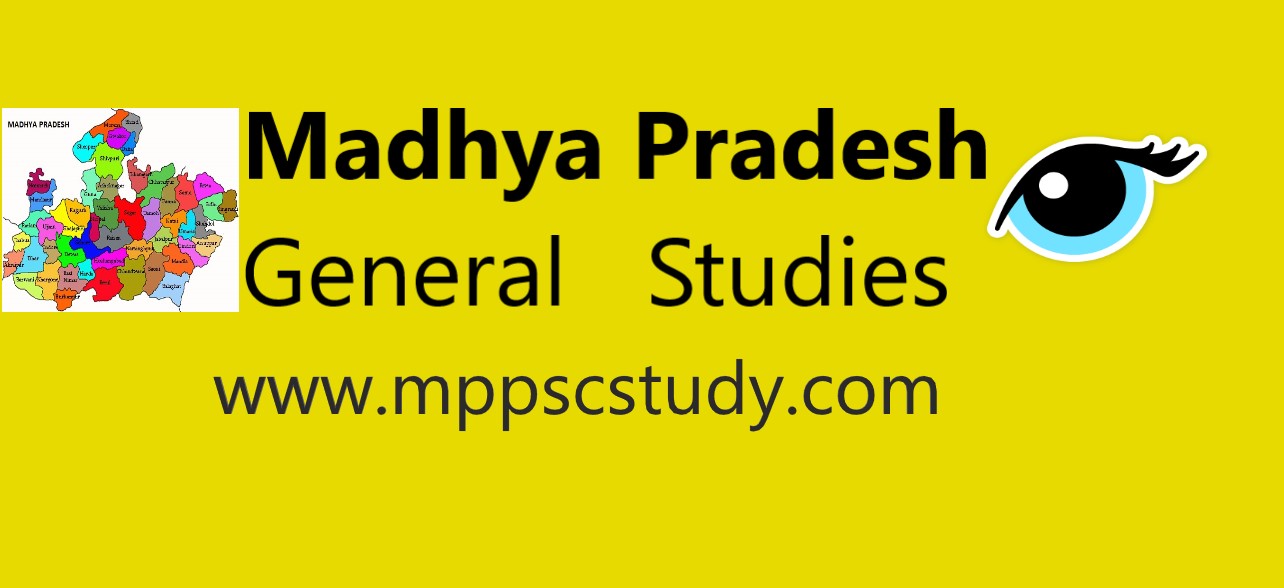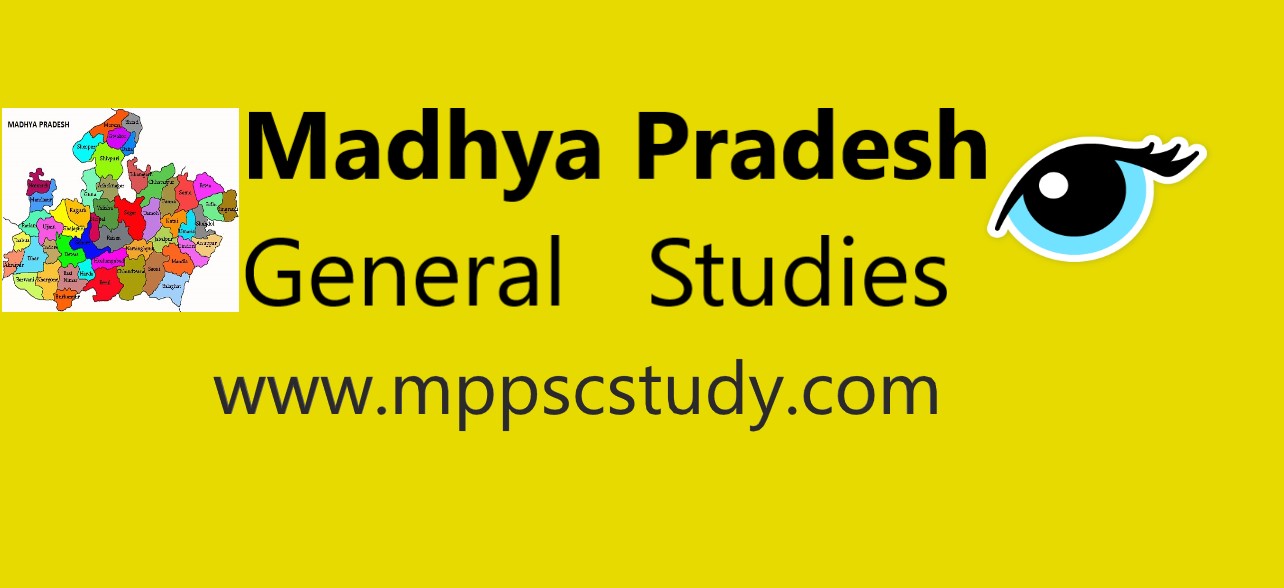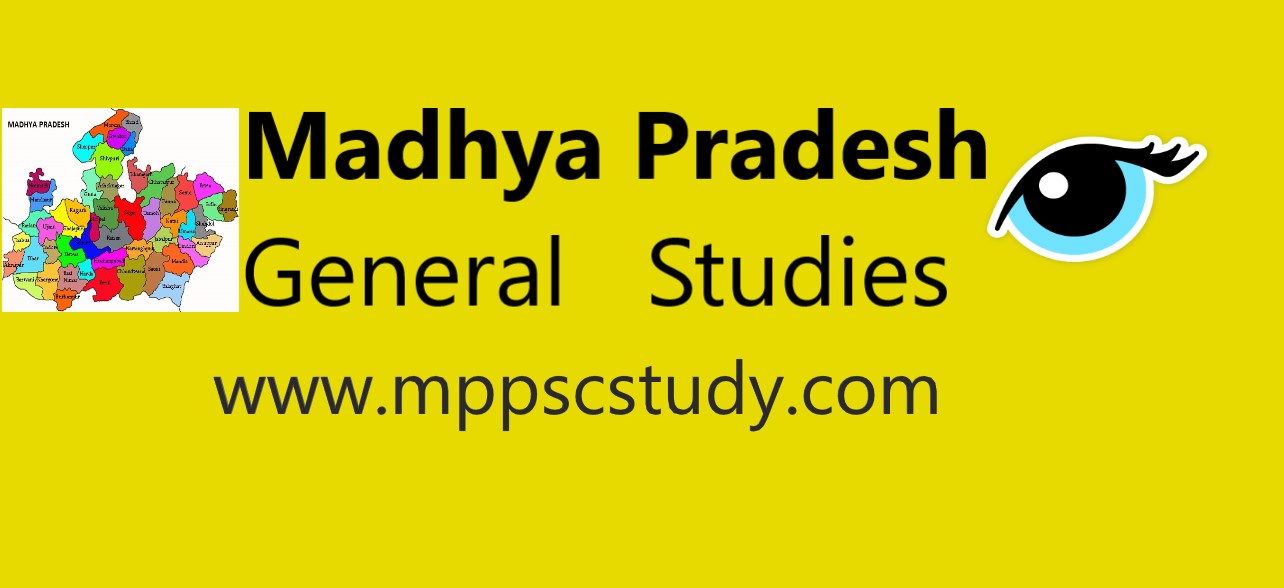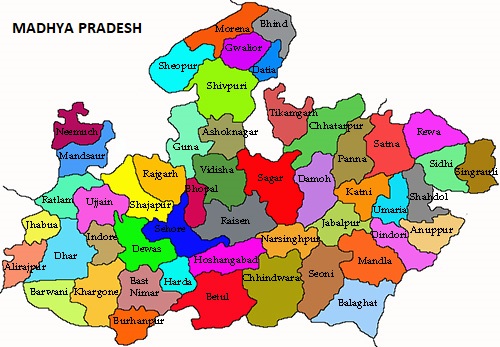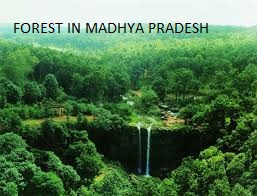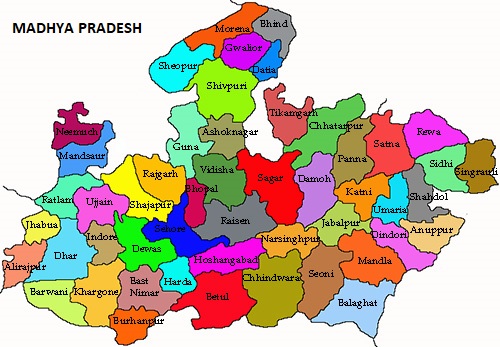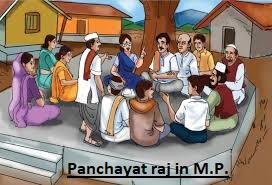डॉ. एनी बीसेंट
जन्म
डा एनी बीसेण्ट का जन्म 1 अक्टूबर 1847 को लंदन में आयरिश मूल के अत्यंत सम्मानित परिवार में हुआ था। उनके बचपन का नाम ऐनीवुड था। वे अपनी उत्कृष्ट पारिवारिक परंपरा के पोषण के लिए अत्यंत सजग थीं।
शिक्षा
पांच वर्ष की उम्र में पिता का साया उठ जाने के बाद उनका जीवन संघर्षपूर्ण हो गया। मां छात्रावास चलाने लगी और उनकी देखभाल का जिम्मा प्रसिद्ध उपन्यासकार कैप्टेन मारयात की बहन को दे दिया। जो उन्हें 14 वर्ष की उम्र में जर्मनी ले गईं। वहां जर्मन भाषा का अध्ययन करने के बाद इंगलैंड आकर संगीत की शिक्षा ग्रहण की।
विवाह
1867 में ऐनी का विवाह रैवरैंड फ्रेंक बीसेण्ट नाम के पादरी से हुआ। धर्म की भावना से ओतप्रोत ऐनी ने पाया कि पादरी होने के बावजूद पति का व्यवहार आदर्श पुरुष की तरह नहीं है जिसकी उन्होंने कल्पना की थी। 1869 व 1870 में क्रमश: पुत्र व पुत्री के जन्म के बाद जीवन में नया प्रकाश आया। कुछ समय बाद बच्चों की मृत्यु व पति के व्यवहार ने उन्हें नास्तिक बना दिया। दामपत्य जीवन के बढते मतभेदों के बाद 1873 में उन्होंने तलाक ले लिया।
सार्वजनिक जीवन
1873 तक उन्होंने जीवन के अगले चरण की तैयारियां शुरु कर दी थीं। चाल्र्स ब्रेडले के प्रति आकर्षित हो चुकी ऐनी ने मि स्काट के लिए पेम्पलेट लिखने शुरु कर दिए।
1875 में श्रीमती बीसेण्ट फ्री थाट सोसायटी के लिए व्याख्यान द्वारा प्रचार कार्य करते हुए जन सामान्य के संपर्क में आईं।
1885 में वे फेबियन सोसायटी की सदस्य बनीं। वे सिडनी वैब, जार्ज बर्नाड शा व ग्राहम वैलेस के संपर्क में आईं। फेबियन सोसायटी की सदस्य के रुप में उन्होंने समाज सुधार के अनेक काम किए। सीक्रेट डाक्टेराइन में मैडम ब्लावैटस्की के विचारों से प्रभावित होकर 1889 में उन्होंने थियोसोफिकल सोसायटी की सदस्यता स्वीकार कर ली। जीवन पर्यंत इस संस्था के साथ जुडी रहीं। 1906 में वे थियोसोफिकल सोसायटी की अध्यक्ष बनीं। इस संस्था से जुडने का अर्थ था कि वे विकासवादी विचारधारा को स्वीकार करती थीं और आस्तिक हो गईं।
भारत आगमन
16 नवंबर 1893 का महत्वपूर्ण दिन था जब श्रीमती बीसेण्ट ने कैंडी में व्याख्यान देकर अपनी भारत यात्रा प्रारंभ की थी। उसके बाद तूतीकोरिन, बंगलौर, आगरा, बैजवाडा, बंबई व लाहौर में धर्म दर्शन के विषयों पर आख्यान दिए और थियासोफी विचारधारा का प्रचार किया। 1901 में नेहरुजी श्रीमती बीसेण्ट से मिले तब उनकी उम्र 12 वर्ष थी।
सेवा कार्य
सन 1193 में भारत आगमन के पूर्व ही सन 1892 में श्रीमती ऐनीबीसेण्ट ने एक पत्र में भारत को अपनी मातृभूमि कहा था। राजनीति के क्षेत्र में उन्होंने लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी, मालवीय जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी आदि के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। 1916 में उन्होंने होमरुल लीग की स्थापना की। इसी संदर्भ में उन्हें 1917 में जेल यात्रा भी करनी पडी। इसी वर्ष वे कांग्रेस की अध्यक्ष बनीं।
श्रीमती ऐनीबीसेण्ट की राजनैतिक दृष्टि बहुत पैनी थी। सन 1920—21 में महात्मा गांधी द्वारा चलाए जा रहे असहयोग आंदोलन एवं खिलाफत आंदोलन का विरोध किया। एवं गांधीजी से मतभेद हो जाने के कारण कांग्रेस छोड दी। उनका कहना था कि—हम देश को स्वतंत्र तो कर लेंगे, परंतु उस पर शासन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अनुशासनहीनता की शक्तियां हमारे युवावर्ग को पूरी तरह जकड लेंगी। बाद में असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी ने स्वयं हिमालयन ब्लंडर या हिमालयी भूल कहा था। खिलाफत का समर्थन करके भी गांधीजी मुसलमानों का दिल नहीं जीत सके और राष्ट्रीय शक्तियां दुर्बल ही हुईं।
श्रीमती ऐनीबीसेण्ट ने भारतीय संस्कृति के उद्धार के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य पुराणों का पुनरुद्धार किया था। उन्होंने माना कि प्रतीक शैली पर लिखे गए पुराण साहित्य ज्ञान के अक्षय भंडार हैं। भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए पुराणों के महत्व को स्वीकार करना होगा।
शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने कई संस्थाओं की स्थापना की। अनेक पुस्तकें लिखी। बाल साहित्य का प्रणयन किया और शिक्षा के वास्तविक रुप को स्पष्ट किया। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी जिसके आधार पर विकसित हुआ, उस हिंदू कालेज की स्थापना का श्रेय श्रीमती बीसेण्ट को ही प्राप्त है। समाज का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें उन्होंने अपना योगदान न दिया हो। उनका मानना था कि भारत को राष्ट्रकुल के सदस्य के रुप में स्वतंत्रता स्वीकार करनी चाहिए। जब 1947 में भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई और वह राष्ट्रकुल का सदस्य बना तब स्वतंत्रत भारत के गर्वनर ने दर्द भरे स्वर में कहा था कि —हमने यदि श्रीमती बीसेण्ट की बात मानी होती तो न देश का विभाजन होता न ही हिंदू मुसलमान दंगे होते। न ही इतना रक्तपात होता। अंतत: भारत राष्ट्रकुल का सदस्य तो बना ही।
सन 1931 व 1932 में होने वाले गोलमेज सम्मेलन से उत्पन्न निराशा ने उनके स्वास्थ्य पर विपरीत असर डाला और वह 20 सितंबर 1933 को परलोकवासी हो गईं। थियोसोफिकल सोसायटी , वाराणसी शांतिकुंज में उनके निवास पर आज भी शांति महसूस की जा सकती है।
मुख्य परीक्षा के लिए सामग्री